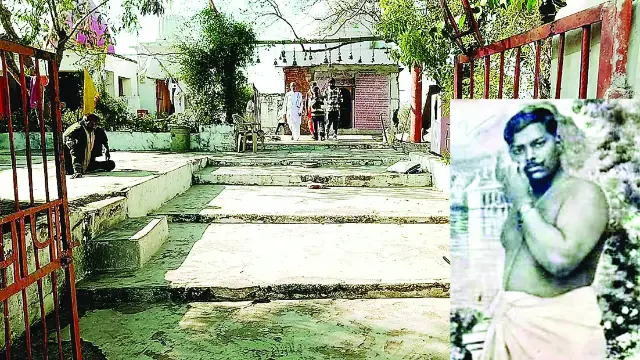1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ शुरू हुई मिसाइल तकनीक में भारत की प्रगति यात्रा
अरुण तिवारी
1970-80 के दशक से शुरू हुई भारत की मिसाइल तकनीक की प्रगति यात्रा दशकों की रणनीतिक दृष्टि, वैज्ञानिक नवाचार और एक व्यापक तंत्र के विकास को दिखाती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के विकास की यह क्रमिक यात्रा 1975 में रूसी रॉकेट द्वारा भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण और 1979 में अपने ही रॉकेट से रोहिणी के प्रक्षेपण जैसे अहम पड़ावों से होकर गुजरी है। बाद के समय में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व और विजन ने देश के मिसाइल कार्यक्रम को दुनिया के विकसित देशों के समानांतर ला खड़ा किया। डॉ. कलाम ने पहली बार अंतरिक्ष में प्रक्षेपण की क्षमता को मिसाइल तकनीक से जोड़ने के रणनीतिक महत्व को पहचाना और जरूरी प्रयोग शुरू किए। उन्होंने आईआईटी और सीएसआईआर के साथ मिलकर शोध शुरू किए। उन्होंने धातु एवं इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में उद्योग जगत की क्षमताओं का इस्तेमाल किया। इसके पीछे उनका उद्देश्य एक ऐसा तकनीकी तंत्र विकसित करना था, जो भविष्य में स्वतंत्र रूप से आधुनिक इंजीनियरिंग समाधान तैयार कर सके।
तकनीकी घटकों के स्वदेशी उत्पादन की चुनौती
उस दौर में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू थे और इन्हें देखते हुए महत्वपूर्ण तकनीकी घटकों के स्वदेशी स्तर पर उत्पादन की बड़ी चुनौती थी। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कॉम्पोजिट मैटेरियल, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ठोस रॉकेट मोटर और सटीक मार्गदर्शन प्रणाली जैसी जटिल तकनीकों के विकास के प्रयास शुरू किए। उनकी मेहनत रंग लाई और भारत इन जटिल तकनीकी घटकों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन में सक्षम हो गया। इसने भारत को अंतरिक्ष प्रक्षेपण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति में ला खड़ा किया। समय के साथ स्थिति बदली और आज भारत, मिसाइल तकनीक का निर्माता और निर्यातक बन गया है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज वाले ठोस-र्इंधन अग्नि मोटर और वायु रक्षा प्रणाली की इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पूरी तरह स्वदेशी रूप से विकसित की गई। रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इस परिवर्तन की मिसाल है, जिसने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत किया और रक्षा उद्योग के निर्यात को प्रोत्साहित किया।
युद्ध की प्रकृति पूरी तरह बदल देंगे तकनीकी बदलाव
भविष्य की ओर देखें तो मिसाइल तकनीक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर में प्रवेश करती दिख रही है। जमीन, जहाजों, पनडुब्बियों या ड्रोन जैसे गतिशील प्लेटफॉर्म, एआई आधारित एल्गोरिद्म अपनाकर अपनी लोकेशन बहुत तेजी से बदलने में सक्षम होंगे और दुश्मन के लिए उन्हें निशाना बनाना और कठिन हो जाएगा। इसी तरह अंतरिक्ष में कई उपग्रहों के समूह तैयार किए जा रहे हैं, जो सेंसरों और एआई बेस्ड विश्लेषण तकनीक से लैस होंगे। ये मिलकर धरती पर किसी ड्रोन, मिसाइल, वाहन आदि को सटीक दिशा निर्देश देने में सक्षम होंगे। इनके मार्गदर्शन से भविष्य के संघर्ष और भयावह हो जाएंगे। मिसाइल तकनीक में होने वाले क्रांतिकारी बदलाव अगले दिनों में युद्ध की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देंगे। तकनीकी सीमाएं जहां युद्ध की रणनीति और प्रतिरोध की प्रकृति में बदलाव करेंगी, वहीं यह वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए नई चुनौतियां भी पेश करेंगी।
स्वायत्त नेविगेशन-उपग्रह प्रणालियां आपदा प्रबंधन में सहायक
इस स्थिति में विभिन्न देशों के बीच एक-दूसरे से आगे निकलने की दौड़ कहां खत्म होगी, इसका अनुमान लगाना डरा देता है। ऐसी तकनीक के नैतिक और रणनीतिक पहलुओं पर गहन मंथन जरूरी होगा, जो भविष्य के युद्ध और वैश्विक स्थिरता पर बहस को आकार देगा। हालांकि, इन तकनीकों का नेतृत्व सैन्य क्षेत्र कर रहा है, लेकिन इनमें कई शांतिप्रिय संभावनाएं भी छिपी हैं। डॉ. कलाम की विरासत इस बात का प्रमाण है कि कैसे सैन्य तकनीक से नागरिक जीवन को लाभ मिल सकता है—जैसे विकलांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण या हृदय रोगियों के लिए स्टेंट। स्वायत्त नेविगेशन और उपग्रह प्रणालियां आपदा प्रबंधन, वैज्ञानिक अनुसंधान और दूरस्थ इलाकों में रसद सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित कर सकती हैं।
एआई आधारित विश्लेषण से सटीक होगा पर्यावरण प्रबंधन
अंतरिक्ष आधारित अवलोकन प्रणालियां जलवायु निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और पर्यावरण प्रबंधन को और बेहतर बना सकती हैं। एआई संचालित डेटा विश्लेषण से शहरी योजना, यातायात प्रबंधन और आपात सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है। इस तरह हम पाते हैं कि देश की मिसाइल यात्रा एक समग्र दृष्टिकोण का उदाहरण है, जिसमें रणनीतिक सोच, तकनीकी नवाचार का सुंदर संयोजन है। यह कुछ ऐसा ही है, जैसे घर का बना भोजन स्वस्थ, किफायती होता है। आने वाले समय में यह न केवल प्रतिरक्षा सामर्थ्य को मजबूत करेगा, बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाएगा बशर्ते तकनीकी प्रगति जिम्मेदारी और नैतिकता के नियंत्रण में रहे।
(पूर्व मिसाइल वैज्ञानिक, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सहयोगी और को-आथर)